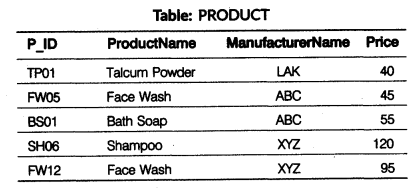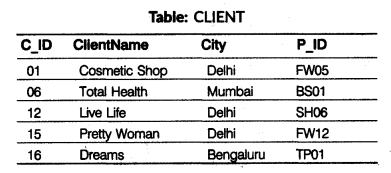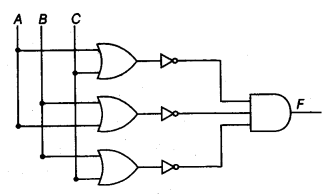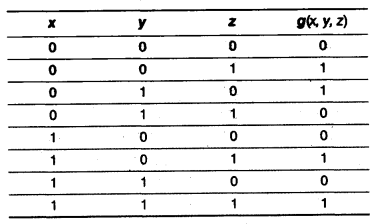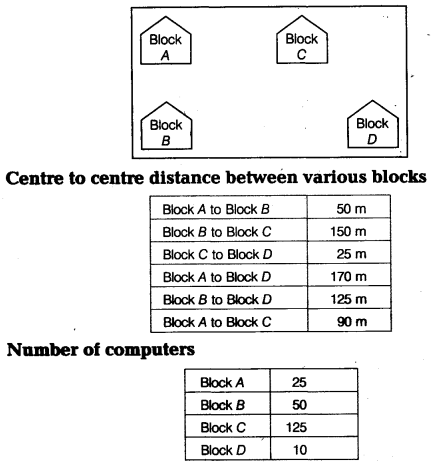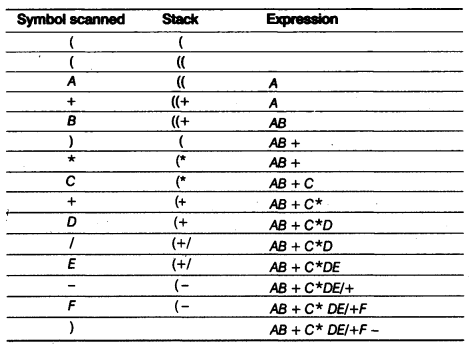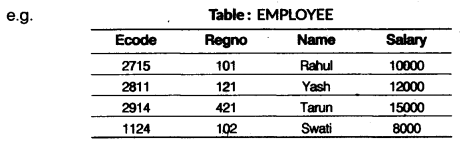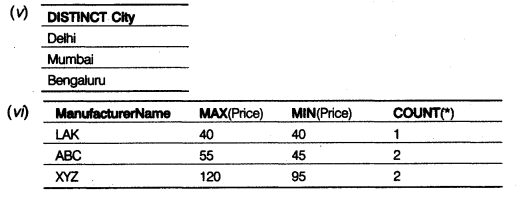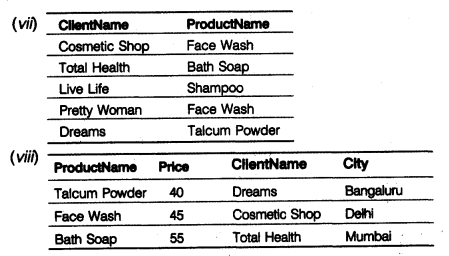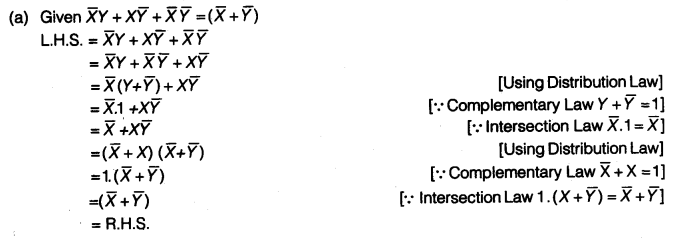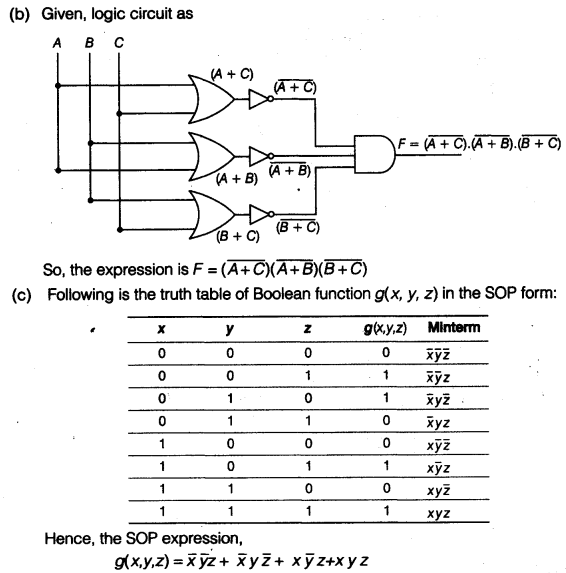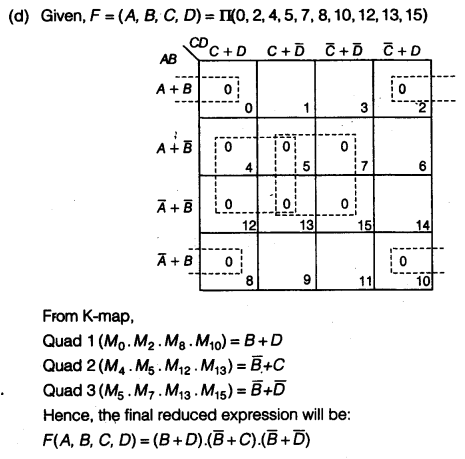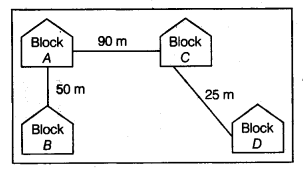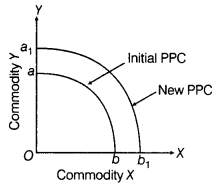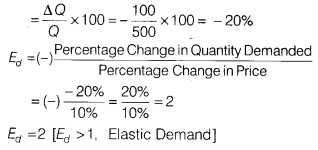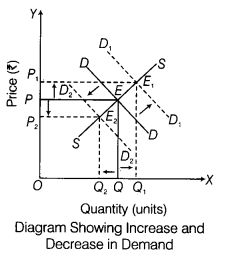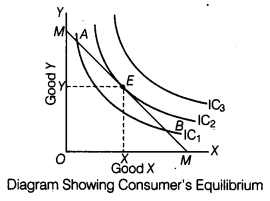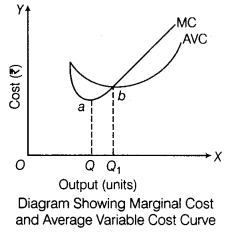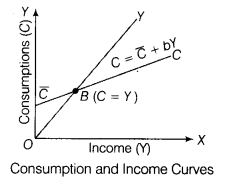CBSE Sample Papers for Class 12 Hindi Paper 3 are part of CBSE Sample Papers for Class 12 Hindi. Here we have given CBSE Sample Papers for Class 12 Hindi Paper 3.
CBSE Sample Papers for Class 12 Hindi Paper 3
| Board | CBSE |
| Class | XII |
| Subject | Hindi |
| Sample Paper Set | Paper 3 |
| Category | CBSE Sample Papers |
Students who are going to appear for CBSE Class 12 Examinations are advised to practice the CBSE sample papers given here which is designed as per the latest Syllabus and marking scheme as prescribed by the CBSE is given here. Paper 3 of Solved CBSE Sample Paper for Class 12 Hindi is given below with free PDF download solutions.
समय :3 घंटे
पूर्णांक : 100
सामान्य निर्देश
- इस प्रश्न-पत्र के तीन खंड हैं-क, ख और ग।
- तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।
- यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए।
प्रश्न 1.
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए (15)
उत्तर-आधुनिक समाज में मनुष्य की सोच सिर्फ स्वयं तक ही सीमित हो गई है। नैतिकता सिर्फ दूसरों को उपदेश देने की वस्तु बनकर रह गई है। आज मनुष्य स्वयं को लाभ पहुँचाने के लिए सभी प्रकार के छल-प्रपंचों का सहारा लेता है। दैनिक जीवन में मानवीय व्यवहार के अंतर्गत एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण गुण सत्य बोलने संबंधी है, जिससे सामाजिक व्यवस्था एवं मानवीय संबंध निर्बाध रूप से निरंतर प्रगतिशील रह सकें। लेकिन एक समय अपनी सत्यवादिता को निभाने वाले राजा हरिश्चंद्र के अतुलनीय त्याग की कल्पना करना भी अब दुर्लभ है, वैसा वास्तविक व्यवहार तो असंभव है। हमारे समाज के निर्माताओं ने सामाजिक मूल्यों में सुत्य बोलने को इतना महत्त्व इसलिए प्रदान किया, क्योंकि मनुष्य अंत:क्रिया करने वाले दूसरे मनुष्यों के साथ छल-कपट न कर सके; समाज के अन्य सदस्य यथार्थ से वंचित एवं भ्रम के शिकार न रहें। यह सामाजिक व्यवस्था को न केवल सुचारु ढंग से परिचालित करने में सहायक है, बल्कि इस सामाजिक मूल्य के माध्यम से समाज अपने सदस्यों को त्याग करने एवं पुरहित को ध्यान में रखने की भी सीख देती है। यह सामाजिक मूल्यों को और उच्च स्तरीय बनाने एवं गरिमा प्रदान करने का भी कार्य करता है। कहा जा सकता है कि सत्य बोलना एक कुंजी अर्थात् आधारभूत सामाजिक मूल्य है, जिससे अन्य सामाजिक मूल्य अंतर्संबंधित हैं।
इसके ठीक विपरीत झूठ बोलना सबसे बड़ा व्यक्तिगत एवं सामाजिक दुर्गुण है। झूठ बोलुना एक प्रकार की चोरी है, जिसमें किसी की दृष्टि से तथ्यों को छिपाया जाता है। यह लोगों को न केवल वास्तविकता से दूर रखता है, बल्कि भावी परिणाम के प्रति भी सतर्क होने से वंचित करता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक स्तर पर समाज एवं दूसरे सदस्यों को क्षति होती है। यह व्यक्ति एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर अत्यधिक नुकसानुदायुक एवं कष्टदायी होता है। यह सामाजिक स्तर पर किया जाने वाला सर्वाधिक नकारात्मक व्यवहार है, क्योंकि इसका प्रभाव वर्तमान के साथ-साथ भविष्य पर भी अत्यंत गंभीर रूप से पड़ता है। झूठ बोलने के कारण व्यक्ति कभी भी वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाता, परिणामस्वरूप वह न तो उसे परिवर्तित करने के लिए कोई प्रयास कर पाता है और न ही संभावित दुष्परिणामों के प्रति सतर्क हो पता है।
इसलिए कहा गया है कि झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ‘पाप’ इस अर्थ में कि यह हमें दिग्भ्रमित करके वांछितु कर्तव्यों से वंचित रखता है। झूठ या असत्य कथन ही बुराइयों की जड़ है। दुनिया में आने वाले किसी बच्चे द्वारा सबसे पहला गलत कार्य झूठ बोलना ही है और यहीं से उसमें भावी अनैतिकताओं एवं अपराधों की नींव पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि झूठ बोलुना सभी पापों का मूल है।2
(क) प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक बताइए। (1)
(ख) उत्तर-आधुनिक समाज में नैतिकता कहाँ तक सीमित हो गई है और क्यों? (2)
(ग) सत्य बोलने तथा मानवीय संबंधों के निरंतर प्रगतिशील होने में क्या संबंध है? (2)
(घ) सत्य बोलना एक आधारभूत सामाजिक मूल्य कैसे है? स्पष्ट कीजिए। (2)
(ङ) “झूठ बोलना एक प्रकार की चोरी है।” पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। (2)
(च) झूठ बोलने को पाप के रूप में देखना कहाँ तक उचित है? (2)
(छ) झूठ को सभी पापों का मूल क्यों कहा गया है? (2)
(ज) गद्यांश का केंद्रीय भाव लगभग 20 शब्दों में लिखिए। (2)
प्रश्न 2.
निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए (1 × 5 = 5)

(क) गलत राह पर चल रहे व्यक्ति को सही राह पर लाने के क्या उपाय हैं?
(ख) प्यार की शक्ति के बारे में कवि की क्या धारणा है?
(ग) प्रस्तुत काव्यांश में प्रयुक्त काव्य-पंक्ति “हर एक धृष्टता के कपोल आँसू से गीले होते हैं”- का आशय स्पष्ट कीजिए।
(घ) अंतर का स्नेह बाँटने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
(ङ) प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न 3.
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए
(क) आपदा प्रबंधन
(ख) ओज़ोन क्षरण का प्राणी जगत पर प्रभाव
(ग) सफलता के लिए शिष्टाचार आवश्यक
(घ) ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन
प्रश्न 4.
भारत के कुछ राज्यों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या बहुत कम है। आप इसका क्या कारण मानते हैं तथा आपकी दृष्टि में इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय हो सकते हैं? किसी दैनिक समाचार-पत्र के संपादक को एक पत्र लिखकर इसे स्पष्ट कीजिए।
अथवा
आपने पत्रकारिता का अध्ययन पूरा कर लिया है। किसी समाचार-पत्र में संवाददाता पद के लिए अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए आवेदन-पत्र लिखिए।
प्रश्न 5.
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए (1 × 5 = 5)
(क) विशेषीकृत पत्रकारिता से क्या समझते हैं?
(ख) हिंदी पत्रकारिता दिवस कब और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
(ग) संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता है?
(घ) ‘वॉचडॉग पत्रकारिता’ किस प्रकार लोकतंत्र का प्रहरी है?
(ङ) जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं?
प्रश्न 6.
‘भारत में बाल मज़दूरी की समस्या’ विषय पर आलेख लिखिए।
अथवा
हाल ही में पढ़ी गई किसी पुस्तक की समीक्षा लिखिए। (5)
प्रश्न 7.
‘आधुनिक समय की गंभीर समस्याः ई-कचरा’ अथवा ‘समाचार पत्र का महत्त्व’ में से किसी एक विषय पर फ़ीचर तैयार कीजिए।
प्रश्न 8.
निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए (2 x 4 = 8)
हँसते हैं छोटे पौधे लघुभार –
शस्य अपार,
हिल-हिल।
खिल-खिल
हाथ हिलाते
तुझे बुलाते
विप्लव-रव से छोटे ही हैं शोभा पाते।
अट्टालिका नहीं है रे
आतंक-भुवन
सदा पुंक पर ही होता
जुल-विप्लवु-प्लावन,
क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से
सदा छलकता नीर,
रोग-शोक में भी हँसता है।
शैशव का सुकुमार शरीर।
(क) ‘विप्लव-रव से छोटे ही हैं शोभा पाते’ का आशय स्पष्ट कीजिए।
(ख) अट्टालिकाओं को ‘आतंक-भवन’ क्यों कहा गया है?
(ग) काव्यांश का केंद्रीय भाव समझाइए।
(घ) प्रकृति बादलों को किस प्रकार बुलाती है और क्यों?
अथवा
आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था
बात सीधी थी पर ज़ोर ज़बरदस्ती से
बात की चूड़ी मुर गई।
और वह भाषा में बेकार घूमने लगी!
हार कर मैंने उसे कील की तरह।
उसी जगह ठोंक दिया।
ऊपर से ठीक-ठाक
पर अंदर से
न तो उसमें कसाव था
नु ताकत!
(क) ‘बात की चूड़ी मर गई’ का आशय स्पष्ट कीजिए।
(ख) भाषा को ‘कील की तरह ठोकने’ से कवि का क्या अभिप्राय है?
(ग) अंदर से कसाव और ताकत न होने का संदर्भ-सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए।
(घ) काव्यांश का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए।
प्रश्न 9.
निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए (2 × 3 = 6)
सवेरा हुआ।
खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा
शरद् आया पुलों को पार करते हुए
अपनी नई चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए
घंटी बजाते हुए ज़ोर-ज़ोर से ।
चमकीले इशारों से बुलाते हुए
(क) प्रातःकाल की तुलना किससे की गई है और क्यों?
(ख) काव्यांश में निहित बिंब को स्पष्ट कीजिए।
(ग) मानवीकरण के सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए।
अथवा
आँगन में तुनुक रहा है ज़िदयाया है।
बालुक तो हई चाँद पै लुलुचाया है।
दर्पण उसे देके कह रही है माँ
देख आईने में चाँद उतर आया है।
(क) प्रस्तुत काव्यांश का भाव-सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए।
(ख) काव्यांश की भाषा एवं छंद की विशिष्टता बताइए।
(ग) देख आईने में चाँद उतर आया है’ कथन के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न 10.
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए (3 × 2 = 6)
(क) ‘आत्म परिचय’ कविता एक ओर “जग-जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर कहती है “मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ”-विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है?
(ख) ‘कैमरे में बंद अपाहिज’ कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि कविता संवेदनहीन सूचना प्रसारण तंत्र पर एक व्यंग्य है।
(ग) ‘कवितावली’ कविता के आधार पर “माँगि के खैबो, मसीत को सोइबो, लैबोको एकु न दैबको दोऊ” काव्य-पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न 11.
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए (2 × 4= 8)
भारतीय कला और सौंदर्यशास्त्र को कई रसों का पता है, उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ-साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है, जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्यू में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की माँग करता है, जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। ‘रामायण’ तथा ‘महाभारत’ में जो हास्य है, वह ‘दूसरों पर है और अधिकांशतः वह पुरसंताप से प्रेरित है, जो करुणा है वह अकसर सद्व्यक्तियों के लिए और कभी-कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राजव्यक्तियों से कुछ बदतमीज़ियाँ अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हँसने और दूसरों में भी वैसा ही मुद्दा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नज़र आती है।
(क) भारतीय कला के बारे में लेखक के क्या विचार हैं?
(ख) विदूषक किसे कहते हैं? इसका क्या महत्त्व है?
(ग) कौन-सी सांस्कृतिक परंपरा भारत में सामान्य रूप से नहीं दिखती?
(घ) भारतीय साहित्य में हास्य संबंधी कौन-सी कमी है?
प्रश्न 12.
निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए (3 × 4 = 12)
(क) लक्ष्मी के भक्तिन बनने की प्रक्रिया मर्मस्पर्शी क्यों है? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए।
(ख) बाज़ार एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। स्पष्ट कीजिए।
(ग) “काले मेघा पानी दे’ पाठ का कौन-सा पात्र इंदर सेना पर पानी फेंका जाना सही ठहराता है? वह उसके पक्ष में क्या-क्या तर्क देता है?
(घ) ‘पहलवान की ढोलक’ कहानी में प्रयुक्त पंक्ति ‘कफ़न की क्या ज़रूरत है’ से क्या अभिप्राय है?
(ङ) राजनीतिक सीमा में बँटे होने के बावजूद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक ही इंसानी दिल के टुकड़े धड़क रहे हैं, जो मिलने को आतुर हैं। ‘नमक’ पाठ के आधार पर इसे स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न 13.
‘सिल्वर वैडिंग’ कहानी में एक ओर स्थिति को ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो दूसरी ओर अनिर्णय की स्थिति भी। कहानी के इस द्वंद्व को स्पष्ट कीजिए। (5)
प्रश्न 14.
(क) क्या सिंधु घाटी सभ्यता को ‘जल संस्कृति’ कह सकते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए।
(ख) जूझ’ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष की प्रेरक कथा है। इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। (5)
उत्तर
उत्तर 1.
(क) प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक ‘सच और झूठ का प्रभाव हो सकता है।
(ख) उत्तर-आधुनिक समाज में नैतिकता सिर्फ दूसरों को उपदेश देने तक सीमित हो गई है, क्योंकि मनुष्य केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, चाहे उसके लिए उसे छल-प्रपंच का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। आज मानव अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों का अहित करने से भी पीछे नहीं रहता है।
(ग) सत्य बोलना एक ऐसा मानवीय गुण है, जिसके कारण आपसी अंतःक्रिया में मनुष्य एक-दूसरे के साथ छल-कपट नहीं कर सकता। इससे समाज के सदस्यों के बीच किसी तरह का भ्रम या अनिश्चय की स्थिति नहीं रहती है। साथ ही, समाज के सदस्य यथार्थ से वंचित नहीं रहते। इसी कारण सामाजिक व्यवस्था एवं मानवीय संबंध निरंतर विकसित होते रहते हैं।
(घ) सत्य बोलना एक कुंजी अर्थात् आधारभूत सामाजिक मूल्य है, क्योंकि इससे अन्य सामाजिक मूल्य संबंधित हैं। वस्तुतः सत्य बोलने की प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य एक-दूसरे पर विश्वास करता है और कही गई बातों के आधार पर ही भविष्य की योजनाएँ निर्धारित की जाती हैं। भाईचारे की भावना के कारण ही मनुष्य एक-दूसरे के लिए त्याग करता है तथा उसके अंदर परहित की भावना उत्पन्न होती है।
(ङ) “झूठ बोलना एक प्रकार की चोरी है।” इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार, चोरी करने की प्रक्रिया में कोई चीज़ छिपाकर सबकी नज़रों से बचाई जाती है, ठीक ऐसी ही प्रवृत्ति झूठ बोलने के दौरान अपनाई जाती है। झूठ बोलने की प्रक्रिया में तथ्यों को छिपाया जाता है, दुनिया के लोगों को वास्तविकता से दूर रखा जाता है। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि झूठ बोलना एक प्रकार की चोरी ही है।
(च) जब कभी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो उससे पूरा समाज या अन्य कोई विशिष्ट व्यक्ति यथार्थ से परिचित नहीं हो पाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि वह न तो उस स्थिति को परिवर्तित करने के लिए कोई प्रयास कर पाता है और न ही संभावित दुष्परिणामों के प्रति सतर्क हो पाता है। इस कारण अन्य व्यक्ति या समाज को अनपेक्षित हानि होती है, जिसे समाप्त करने या कम करने का उसे अवसर ही नहीं मिल पाता है। इस संदर्भ में झूठ बोलने को पाप के रूप में देखना औचित्यपूर्ण है।
(छ) प्रस्तुत गद्यांश में स्पष्ट किया गया है कि दुनिया में कदम रखने वाले किसी भी बच्चे द्वारा सबसे पहला गलत कार्य उसके झूठ बोलने से ही प्रारंभ होता है। झूठ बोलना प्रारंभ करके ही वह गलत मार्ग की ओर अग्रसर होता है और यहीं से उसकी भावी अनैतिक गतिविधियों तथा अपराध करने की शुरुआत होती है। इस कारण झूठ को सभी पापों का मूल कहा गया है।
(ज) गद्यांश का केंद्रीय भाव यह है कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य के आधार पर ही सामाजिक मूल्य उच्च स्तरीय तथा गरिमामय रूप में स्थापित होते हैं, जबकि झूठ के आधार पर मनुष्य गलत मार्ग की ओर अग्रसर होता है, जिससे व्यक्ति के साथ समाज का भी अहित होता है।
उत्तर 2.
(क) प्रस्तुत काव्यांश के अनुसार, गलत राह पर चल रहे व्यक्ति को प्रेम, अपनापन, सहानुभूति आदि से भरे व्यवहार द्वारा समझाकर सही मार्ग पर लाया जा सकता है।
(ख) कवि की धारणा है कि प्यार में वह शक्ति होती है, जो किसी भी प्रकृति के व्यक्ति को उचित एवं अभीष्ट मार्ग पर ले आए। इसके माध्यम से संसार की सभी बुराइयों को दूर तथा अच्छाइयों का प्रतिस्थापन किया जा सकता है।
(ग) प्रस्तुत काव्यांश में काव्य-पंक्ति “हर एक धृष्टता के कपोल आँसू से गीले होते हैं” का आशय यह है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा या दुष्ट क्यों न हो, उसके अंदर भी एक हृदय होता है, जो भावनाओं से भरा होता है।
(घ) प्रस्तुत काव्यांश में स्पष्ट किया गया है कि अंतर का स्नेह बाँटने से व्यक्ति का स्थान और अधिक ऊँचा हो जाता है, इससे व्यक्ति का जीवन पूर्व की अपेक्षा अधिक सहज एवं लोक कल्याणकारी बन जाता है।
(ङ) प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव यह है कि प्रेम या स्नेह का लोगों के बीच अधिक-से-अधिक संचार करना चाहिए। मानव समाज की विशिष्टता उसकी मानवीयता में ही निहित है। इन मानवीय गुणों का मूल मानव के अंदर व्याप्त प्रेम की भावना है, जो सभी में मौजूद है।
उत्तर 3.
(क) आपदा प्रबंधन
आपदा से निपटने की तैयारी आपदा प्रबंधन कहलाती है। आपदा एक ऐसी स्थिति है, जिसमें जीवन का सामान्य कर्म बिगड़ जाता है। और मनुष्य एवं पर्यावरण के बचाव हेतु तत्काल बड़े स्तर पर सहायता आवश्यक होती है। आपदाएँ प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित दोनों ही प्रकार की होती हैं।
प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न आपदाएँ ‘प्राकृतिक आपदा’ की श्रेणी में आती हैं; जैसे-आँधी, तूफ़ान, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप आदि। इसी प्रकार मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जनित आपदा मानव-निर्मित या मानव-जनित आपदा कहलाती है। ऐसी आपदाएँ प्रायः असावधानी अथवा अज्ञानता के कारण घटती हैं। उदाहरण के लिए; आग लगना, हानिकारक रसायन का रिसाव होना आदि। भोपाल-गैस दुर्घटना मानवीय आपदा का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपदाओं से बहुत-सी हानियाँ होती हैं, जिन्हें तीन प्रकारों में बाँटा जा सकता है-प्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव तथा गौण प्रभाव। इसके मुख्य चरण हैं-पूर्व में ही बचाव योजना बनाना, प्रबंधन करना, विभिन्न संस्थाओं के मध्य तालमेल स्थापित करना तथा आपदा के समय प्रभावी ढंग से बचाव प्रक्रिया को अंजाम देना।
आपदा के बाद पुनर्वास के लिए काम करना भी आपदा प्रबंधन विभाग का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। आपदा प्रबंधन प्रणाली आपदा को घटने से रोक तो नहीं सकती, लेकिन आपदा आने से पूर्व लोगों को जागरूक करके तथा राहत कार्यों को सही समय पर क्रियान्वित करके आपदा के कारण होने वाले दुष्प्रभावों एवं हानि को कम ज़रूर कर सकती है। इसलिए आपदा प्रबंधन महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन के कारण हम विभिन्न आपदाओं का डटकर सामना कर सकेंगे तथा उनके दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। इससे देश को आगे बढ़ने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी।
(ख) ओज़ोन रण का प्राणी-जुगत पर प्रभाव
ओज़ोन गैस के आवरण को ‘पृथ्वी का रक्षा कवच’ कहा जाता है। ओज़ोन गैस पृथ्वी के चारों ओर समतापमंडल में १५ से ३५ किमी के बीच विद्यमान है। ओज़ोन परत, ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनती है। यह पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की ख़तरनाक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। सूर्य की ये पराबैंगनी किरणें प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इस प्रकार ओज़ोन परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह पाया गया है कि ओज़ोन परत का क्षरण तीव्र गति से हो रहा है। ओज़ोन परत के क्षय के कई कारण हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है औद्योगीकरण| औद्योगीकरण ने। वातावरण को अत्यंत प्रदूषित कर दिया है, जिससे पर्यावरण में ऐसे तत्त्वों की वृद्धि हुई है, जो ओज़ोन परत के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं।
ओज़ोन परत के क्षरण के कई घातक परिणाम सामने आ रहे हैं। यदि इसका क्षय समय रहते नहीं रोका गया, तो इसके और भी घातक परिणामों के सामने आने की आशंका है। इसके कारण पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की पराबैंगनी किरणों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे समस्त प्राणी जगत को हानि पहुँचेगी। ओज़ोन परत की अनुपस्थिति में जीव-जंतुओं तथा मनुष्यों को त्वचा संबंधी अनेक प्रकार के गंभीर तथा जानलेवा रोगों का सामना करना पड़ेगा, पेड़-पौधों का विकास बाधित होगा, पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि होगी, परिणामतः पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा और जीवन संकट में पड़ जाएगा। ओज़ोन परत का संरक्षण करना अति आवश्यक है। हमें समय रहते ओजोन परत का क्षय रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे और ओजोन परत के क्षरण के भावी खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा।
(ग) अफलता के लिए शिष्टाचार आवश्यक
‘शिष्ट’ और ‘आचार’ शब्द के मेल से बना ‘शिष्टाचार’ शब्द हमारे जीवन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अभिप्राय सभ्य एवं उचित व्यवहार करने से है। यह सर्वमान्य है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ-साथ शिष्ट व्यवहार का होना भी आवश्यक है। कहा जाता है कि व्यक्ति का आचरण जैसा होगा, उसी के अनुकूल उसे परिणाम भी प्राप्त होगा। अपने सद् आचरण एवं व्यवहार कुशलता के कारण कम योग्यता वाला व्यक्ति भी तेज़ी से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है और कोई अधिक योग्यता वाला व्यक्ति भी उचित व्यवहार के अभाव में जीवनभर असफल ही रह सकता है।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस कारण उसके लिए शिष्टाचार का महत्त्व एवं उसकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। शिष्टाचार व्यक्ति को अनुशासन की प्रेरणा देता है। अनुशासन के बिना समाज में अराजकता तथा अव्यवस्था का फैलना स्वाभाविक है। अतः हमें सार्वजनिक स्थलों पर शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ एक ओर शिष्टाचार हमारे व्यक्तित्व में चार चाँद लगा देता है, वहीं दूसरी ओर अशिष्ट आचरण हमारे लिए अनेक बाधाएँ तथा कठिनाइयाँ उत्पन्न करने के साथ हमारी सामाजिक गरिमा को नष्ट कर देता है। शिष्टाचार-रहित व्यवहार तथा आचरण, लड़ाई-झगड़े, युद्ध तथा गलतफ़हमी आदि के कारण बनते हैं।
जीवन में सफलता हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में शिष्टाचार का पालन करे और आने वाली पीढ़ी को भी शिष्टाचार का पाठ पढ़ाए। शिष्टाचार के अभाव में अनुशासन भी नहीं रह पाता और अनुशासन के अभाव में समाज में कई प्रकार की बुराइयाँ अपनी जड़ें मज़बूत कर लेती हैं। अतः हमें स्वयं तथा सामाजिक हित के लिए शिष्टाचार के गुण को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि शिष्टाचार जीवन में सफलता का निर्णायक मापदंड है।
(घ) ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन
ऑनलाइन शॉपिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे विभिन्न प्रकार के उत्पादों को खरीदना| ऑनलाइन शॉपिंग से आप घर बैठे मनचाही वस्तु मँगा सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप वस्तु की कीमत अदा, अपनी ऑर्डर की हुई वस्तु के मिल जाने पर कर सकते हैं। देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग समय की बचत करने का एक असरदार तरीका है। हमारे देश में फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ईबे डॉट इन, स्नैप डील डॉट कॉम, होम शॉप आदि कंपनियाँ ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। विशेषकर महानगरों में लोगों को घर बैठे ऑनलाइन चीजें पसंद करना एवं उन्हें मँगाना सुविधाजनक लगने लगा है। आने वाले समय में इसका दायरा किस तरह बढ़ेगा, इसकी आहट बाजार में दिखने लगी है।
ऑनलाइन शॉपिंग के तेज़ी से बढ़ते प्रचलन से पता चलता है कि उपभोक्ताओं की मानसिकता एवं खरीदारी का तरीका तेज़ी से बदल रहा है। पारंपरिक बाज़ारों में खरीदारी की तुलना में ऑनलाइन शॉपिंग का प्रचलन बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं।
- होम डिलीवरी ऑनलाइन शॉपिंग का एक अन्य प्रमुख आकर्षण होम डिलीवरी है। लोगों को उत्पाद खरीदकर लाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती और न ही इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है।
- उत्पाद चयन हेतु पर्याप्त विकल्प ऑनलाइन शॉपिंग की एक अन्य प्रमुख खूबी यह है कि इसमें खरीदारी के लिए उत्पाद के विभिन्न विकल्प मौजूद रहते हैं, जिनकी सभी विशेषताओं को सही ढंग से जानकर अपनी आवश्यकता के अनुसार उनमें से किसी वस्तु का चयन किया जा सकता है।
- कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा ऑनलाइन शॉपिंग में कैश ऑन डिलीवरी अर्थात् उत्पाद प्राप्त होने पर पैसा देना होता है।
- किस्तों पर खरीदारी की सुविधा ऑनलाइन शॉपिंग में अनेक रिटेलर्स द्वारा लोगों को किस्तों पर खरीदारी करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे उपभोक्ता की जेब पर एक साथ बोझ नहीं पड़ता।
- विभिन्न प्रकार के आकर्षक प्रस्ताव ऑनलाइन शॉपिंग में कई तरह के ऑफर्स (प्रस्ताव) भी दिए जाते हैं। एक उत्पाद खरीदने पर दूसरा मुफ़्त या उत्पाद के मूल्य पर अतिरिक्त छूट, जैसे लाभ भी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आकर्षित करते हैं।
हालाँकि इंटरनेट की दुनिया में धोखाधड़ी और जालसाजी की घटनाएँ भी कम नहीं होतीं। अतः हमें सतर्कतापूर्वक ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए और विश्वस्त कंपनियों की ही सेवा प्राप्त करनी चाहिए। इस तरह, आप निश्चय ही ऑनलाइन शॉपिंग को ‘ऑफलाइन शॉपिंग’ से बेहतर पाएँगे।
उत्तर 4.
परीक्षा भवन,
दिल्ली।
दिनांक 12 सितंबर, 20××
सेवा में,
संपादक महोदय,
हिंदुस्तान टाइम्स,
नई दिल्ली।
विषय भारत में घटते लिंगानुपात के संबंध में।
महोदय,
मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार-पत्र के माध्यम से भारत में घटते लिंगानुपात के संबंध में लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज भारत में लिंगानुपात तेज़ी से घट रहा है और कुछ राज्यों में तो यह खतरनाक स्थिति तक पहुँच गया है। घटते लिंगानुपात को सबसे महत्त्वपूर्ण कारण कन्या भ्रूण हत्या है, जिसे विकसित तकनीक का सहारा लेकर बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा रहा है। कन्या भ्रूण-हत्या के पीछे सबसे बड़ी वज़ह सामान्य भारतीयों में पुत्र-प्राप्ति की लालसा है। पढ़े-लिखे समाजों में भी यह आकांक्षा उसी स्तर पर है, जो अशिक्षित समाजों में व्याप्त है। कन्या भ्रूण हत्या के पीछे आर्थिक निर्धनता एवं अशिक्षा भी प्रमुख वज़ह मानी जाती हैं।
वास्तव में, यह प्रवृत्ति हमारे कुत्सित विचारों एवं संकीर्ण मान्यताओं के कारण फल-फूल रही है। लड़कों की तुलना में हम लड़कियों को हीन मानते हैं तथा भविष्य के लिए लड़कियों को बोझ समझते हैं। यदि इस तरह की मानसिक विकृतियों को समय रहते रोका नहीं गया, तो समाज को इससे उत्पन्न प्रभाव का सामना करना पड़ेगा।
इस कुप्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार को सख्ती से कदम उठाने चाहिए तथा जनसामान्य को भी सक्रिय रूप से आगे आना चाहिए। लिंग संबंधी किसी भी तरह के परीक्षण पर तत्काल सख्ती से पूर्णतः रोक लगानी चाहिए तथा जनसामान्य के बीच शिक्षा का अधिक-से-अधिक प्रसार करना चाहिए। कन्या वर्ग को शिक्षा, नौकरी, अनुदान आदि क्षेत्रों में विशेष सुविधाएँ देनी चाहिए तथा लोगों के बीच इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे पुरुषों और महिलाओं के बीच के इस अंतर को कम किया जा सके।
आशा है कि जनहित में आप इसे प्रकाशित करने की कृपा करेंगे।
सधन्यवाद।
भवदीय
क.ख.ग.
अथवा
परीक्षा भवन,
दिल्ली।
दिनांक 19 सितंबर, 20××
सेवा में,
संपादक महोदय,
नवभारत टाइम्स,
बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली।
विषय संवाददाता पद के आवेदन हेतु।
महोदय,
आपके समाचार-पत्र के संवाददाता विभाग ने संवाददाता की नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए हैं। मैं भी इस पद के लिए अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।
मेरा विवरण इस प्रकार है।
नाम सुंदर श्याम
पिता का नाम श्री मनोहर कृष्ण
जन्मतिथि 17 मई, 19××

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कार्य को पूरी योग्यता, ईमानदारी एवं निष्ठा से करूंगा। आशा है कि आप मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करेंगे।
सधन्यवाद।
भवदीय
क.ख.ग.
उत्तर 5.
(क) किसी क्षेत्र विशेष की गहन जानकारी देना और विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। पत्रकारिता में विषय के अनुसार विशेषता के सात क्षेत्र हैं–संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन तथा फ़िल्म पत्रकारिता।
(ख) भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी तारीख को सन् 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने देश का पहला हिंदी समाचार-पत्र ‘उदंत मार्तंड’ प्रकाशित किया था। प्रत्येक मंगलवार को छपकर आने वाले इस साप्ताहिक समाचार-पत्र का प्रकाशन कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) से किया गया था।
(ग) संपादकीय किसी समाचार-पत्र की विचारधारा का संवाहक होता है। यह व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण को प्रस्तुत न करके, उस समाचार-पत्र या समूह के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। यही कारण है कि संपादकीय में प्रायः लेखक का नाम नहीं दिया जाता है।
(घ) लोकतंत्र में पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है। सरकार के कामकाज की गड़बड़ियों का पर्दाफ़ाश करना ही ‘वॉचडॉग पत्रकारिता’ कहलाती है। सरकारी अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं को जनता के बीच ले जाने के माध्यम से यह सरकार पर नियंत्रण रखती है। इससे लोकतंत्र की व्यवस्था एवं मर्यादा बनी रहती है।
(ङ) जब व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की अपेक्षा किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाती है तथा इसकी पहुँच व्यापक स्तर पर होती है, तो इसे जनसंचार माध्यम कहा जाता है; जैसे-रेडियो, दूरदर्शन, समाचार-पत्र, इंटरनेट आदि।
उत्तर 6.
भारत में बाल मजदूरी
‘बाल मज़दूरी’ से तात्पर्य ऐसी मज़दूरी से है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे किसी संस्थान में कार्य करते हैं। जिस आयु में उन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उस आयु में वे किसी दुकान, रेस्टोरेंट पटाखे की फैक्ट्री, हीरे तराशने की फैक्ट्री, शीशे का सामान बनाने वाली फैक्ट्री आदि में काम करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में बाल मज़दूरी के अनेक कारण हैं। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा का महत्त्व न समझ पाने के कारण अपने बच्चों को मज़दूरी करने के लिए भेज देते हैं। जनसंख्या वृद्धि बाल मज़दूरी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। निर्धन परिवार के सदस्य पेट भरने के लिए छोटे-छोटे बच्चों को काम पर भेज देते हैं। भारत में बाल मज़दूरी को गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण इसे प्रोत्साहन मिलता है। देश में कार्य कर रही सरकारी, गैर-सरकारी और निजी संस्थाओं की बाल मजदूरी को दूर करने में गंभीर रुचि की कमी है। बाल मज़दूरी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कड़े कानून बना सकती है। समाज के निर्धन वर्ग को शिक्षा प्रदान करके बाल मज़दूरी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके भी बाल मज़दूरी को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जो बाल मज़दूरी का विरोध करती हैं या बाल मज़दूरी करने वाले बच्चों के लिए शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम चलाती हैं।
अथवा
प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉ. राही मासूम रज़ा के उपन्यास ‘आधा गाँव’ की समीक्षा
हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार डॉ. राही मासूम रज़ा द्वारा लिखित उपन्यास ‘आधा गाँव’ पहली बार वर्ष 1966 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास हिंदी के कथा-साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर’ है। यह एक समर्थ आँचलिक उपन्यास है।
‘आधा गाँव’ उपन्यास को परंपरागत औपन्यासिक ढाँचे को तोड़ने वाला उपन्यास कहा गया है। उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के अँचल गंगोली के शिया मुसलमानों के जीवन को अनेक विसंगतियों के बीच इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। उपन्यासकार इस अँचल को एक ऊँघते परिवेश में चित्रित करता है, जो इतिहास से बेख़बर है और जिसमें भविष्य की कोई कल्पना नहीं। उपन्यास में ही लेखक की ओर से कहा गया है कि वह जो कहानी कह रहा है, वह जितनी सच्ची है, उतनी ही झूठी भी, क्योंकि यह बनी-बनाई कहानी नहीं है, बल्कि सचमुच जीने योग्य कहानी है-”यह उम्रों के हेर-फेर में फँसे हुए सपनों और हौसलों की कहानी है। यह कहानी उन खंडहरों की है, जहाँ कभी मकान थे और यह कहानी उन मकानों की है, जो खंडहरों पर बनाए गए हैं।”
उपन्यास के अंतर्गत विभिन्न रोचक शीर्षकों में राही मासूम रज़ा एक आँचलिक परिवेश बुनते हैं, जैसे-मियाँ लोग, ताना-बाना, नमक गाथा, प्यास-तन्हाई आदि। लेखक इस उपन्यास में शिया मुसलमानों के घरों की अंतरंग जिंदगी और संबंधों में प्रवेश करता है। उपन्यास की भाषा का ठेठपन इसका सर्वाधिक विशिष्ट आकर्षण है तथा सीधे-सच्चे मनुष्यों की ज़बान से निकली गालियों ने भी आँचलिक परिवेश को और अधिक मुखर कर दिया है।
भारतीय समाज के ग्रामीण परिवेश का ताना-बाना तथा हिंदू-मुस्लिम संबंधों की गहराई को समुचित ढंग से समझने तथा तार्किक मूल्यांकन करने के लिए सभी के द्वारा यह उपन्यास पढ़े जाने योग्य है।
उत्तर 7.
आधुनिक समय की गंभीर समस्या : ई-कचरा
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अर्थात् ई-कचरा आधुनिक समय की एक गंभीर समस्या है। वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। इसके फलस्वरूप, आज नित नए-नए उन्नत तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का उत्पादन हो रहा है। जैसे ही बाज़ार में उन्नत तकनीक वाला उत्पाद आता है, वैसे ही पुराने यंत्र बेकार पड़ जाते हैं। इसी का नतीजा है कि आज कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टीवी, रेडियो, प्रिंटर, आई-पोड्स आदि के रूप में ई-कचरा बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार एक वर्ष में पूरे विश्व में लगभग 50 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न होता है। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि ई-कचरे का निपटान उस दर से नहीं हो पा रहा है, जितनी तेज़ी से यह पैदा हो रहा है। बहुत कम मात्रा में ही ई-कचरे का निपटान हो पाता है। शेष कचरा या तो लैंडफिल साइट्स में डाल दिया जाता है या खुले में जला दिया जाता है। इससे पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में आर्सेनिक, कोबाल्ट, मरकरी, बेरियम, लिथियम, कॉपर, क्रोम, लेड आदि हानिकारक अवयव होते हैं। इन्हें खुले में जलाना या मिट्टी में दबाना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ गया है।
अब समय आ गया है कि ई-कचरे के उचित निपटान और पुनः चक्रण पर ध्यान दिया जाए अन्यथा पूरी दुनिया शीघ्र ही ई-कचरे का ढेर बन जाएगी। इसके लिए विकसित देशों को आगे आना होगा और विकासशील देशों के साथ अपनी तकनीकों को साझा करना होगा, क्योंकि विकसित देशों में ही ई-कचरे का उत्पादन अधिक होता है और वे जब-तब चोरी-छिपे विकासशील देशों में उसे भेजते रहते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक होना होगा।
अथवा
समाचार-पत्र का महत्त्व
हमारा समाज परिवर्तनशील समाज है। समय के साथ-साथ समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। विभिन्न परिवर्तनों की सूचना देना और हमारी ख़बर लेने का सबसे सरल और सस्ता माध्यम समाचार-पत्र है। आज प्रत्येक पढ़ा-लिखा व्यक्ति समाचार-पत्र पढ़ता है। उसे सुबह उठते ही समाचार-पत्र पढ़ने की आदत होती है और विश्वभर में फैले संवाददाता एवं संवाद एजेंसियाँ समाचार एकत्र करके समाचार-पत्रों के कार्यालयों में भिजवाती हैं। फिर संपादक इनका संपादन करके प्रकाशन योग्य बनाते हैं। समाचार-पत्र को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। समाचार-पत्र लोगों को जागरूक बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने का सशक्त माध्यम है। सरकारी घपलों का पर्दाफ़ाश करने और सरकार के क्रियाकलापों का कच्चा चिट्ठा खोलने में भी उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण रहती है। हमें घर बैठे ही समाचार-पत्रों से विश्वभर की जानकारी मिल जाती है। जानकारी के अतिरिक्त और बहुत कुछ समाचार-पत्रों में होता है; जैसे-ज्ञानवर्द्धक लेख, संपादकीय लेख, अन्य विद्वानों द्वारा लिखे गए लेख आदि। समसामयिक विषयों पर अनेक प्रासंगिक चर्चा भी इनमें मौजूद रहती है। इसके अलावा इसमें मनोरंजन सामग्री भी प्रकाशित होती है, जिसमें कहानियाँ, चुटकुले, कविताएँ आदि शामिल रहते हैं।
उत्तर 8.
(क) ‘विप्लव-रव से छोटे ही हैं शोभा पाते’ से कवि का आशय है कि बादल जल के रूप में जो विप्लव अर्थात् हलचल उत्पन्न करते हैं, उससे छोटे पौधे अर्थात् समाज के निम्न वर्ग के लोग सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं। विप्लव का दूसरा अर्थ क्रांति से है। कवि का अभिप्राय यह है कि समाज का शोषित, दमित एवं वंचित वर्ग ही सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति का सूत्रधार बनता है तथा उसके लाभों से सबसे अधिक वही जुड़ता है अर्थात् उसे ही सर्वाधिक लाभ होता है।
(ख) अट्टालिकाओं को ‘आतंक-भवन’ इसलिए कहा गया है, क्योंकि अट्टालिकाओं को धनी एवं शोषक वर्ग के निवासस्थान के रूप में चित्रित किया गया है। कवि का मानना है कि इन अट्टालिकाओं में उन शोषक वर्गों का निवास है, जिन्होंने अपने धन एवं सामर्थ्य के बल पर समाज के अधिकांश शोषितों का शोषण करके इस समाज में अपना आतंक कायम किया है।
(ग) काव्यांश में कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि समाज में होने वाली प्रत्येक क्रांति से सबसे अधिक निम्न वर्ग ही प्रभावित होता है। शोषक वर्ग अपनी अट्टालिकाओं (ऊँचे भवनों) में क्रांति से उत्पन्न भय के आवेश में रहता है, फिर भी उस पर क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
(घ) प्रस्तुत काव्यांश के अनुसार, प्रकृति बादलों को प्रसन्नतापूर्वक हाथ हिला-हिलाकर बुलाती है। वस्तुतः बादलों के बरसने से पहले चलने वाली हवा से छोटे पौधे एवं फ़सलें हँसते एवं लहराते जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। कवि कहता है कि प्रकृति बादलों को इसलिए बुलाती है, क्योंकि ये बादल ही वर्षा लाकर किसान की पीड़ा को दूर कर सकते हैं तथा समाज में क्रांति का बिगुल बजा सकते हैं।
अथवा
(क) प्रस्तुत काव्य-पंक्ति ‘बात की चूड़ी मर गई’ एक मुहावरेदार प्रयोग है। कवि कहना चाहता है कि अभिव्यक्ति या काव्य के लिए उचित एवं सरल भाषा का चुनाव न कर पाने की स्थिति में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। वह निरर्थक एवं प्रभावहीन हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपनी कोई बात ज़बरदस्ती कहना या थोपना चाहते हैं, तो वह अपना प्रभाव खो देती है।
(ख) भाषा को ‘कील की तरह ठोकने’ से कवि का अभिप्राय यह है कि अभिव्यक्ति के लिए उचित शब्द या माध्यम न मिल पाने की स्थिति में कवि ने अपनी बात को उलझी हुई स्थिति में ही छोड़ दिया। उसकी अस्पष्टता यथावत् बनी रही। उसकी कसावट समाप्त हो जाने से उसका प्रभाव क्षीण हो गया, हालाँकि बाह्य सुंदरता वैसी ही बनी रही।
(ग) प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कथ्य या अभिव्यक्ति के संदर्भ में यह स्पष्ट करना चाहा है कि भाषा में अंदर से कसावट एवं ताकत न होने का अर्थ अभिव्यक्ति या कथ्य की निरर्थकता एवं निरुद्देश्यता है। भावों के स्पष्ट न होने पर कोई भी बात महत्त्वहीन होकर केवल शब्दाडंबर या शब्दों का जाल बनकर रह जाती है। उसकी प्रभावकारी क्षमता समाप्त हो जाती है।
(घ) प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा के साथ सावधानी बरतते हुए स्वाभाविक रूप से उसका व्यवहार करना चाहिए अर्थात् परिस्थितियों एवं संदर्भो के अनुरूप सोच-समझकर सदा सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। निरर्थक एवं अप्रासंगिक शब्दों का प्रयोग भाषा को प्रभावहीन बना देता है।
उत्तर 9.
(क) प्रस्तुत काव्यांश में प्रातःकाल की तुलना खरगोश की लाल आँखों से की गई है, क्योंकि शरद् ऋतु का प्रातःकालीन सूर्य चमकीला लाल होता है और खरगोश की लाल आँखों जैसा प्रतीत होता है। कवि ने यहाँ प्रातःकाल का चित्रण करने के लिए दृश्य बिंब का सहारा लिया है, जो अत्यंत प्रासंगिक एवं अर्थपूर्ण है।
(ख) काव्यांश में बिंब योजना अत्यंत नवीन एवं आकर्षक है। इसमें दृश्य एवं श्रव्य बिंबों का प्रयोग किया गया है। कवि ने एक ओर शरद् ऋतु के सवेरे की तुलना खरगोश की चमकीली लाल आँखों से करते हुए दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है, तो दूसरी ओर श्रव्य बिंब का प्रयोग करते हुए कहा है कि शरद् का सवेरा ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेज़ गति से चलाते हुए घंटी बजाकर शोर मचाते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है।
(ग) प्रस्तुत काव्यांश में शरद् ऋतु का मानवीकरण विभिन्न बिंबों के माध्यम से किया गया है। खरगोश की लाल आँखों जैसा सवेरा, चमकीली साइकिल की घंटी बजाते हुए तेज़ गति से शरद् ऋतु के सवेरे का आना आदि में मानवीकरण अलंकार मौजूद है, क्योंकि यहाँ निर्जीव शरद् ऋतु के सवेरे पर विभिन्न मानवीय गतिविधियों का आरोपण किया गया है।
अथवा
(क) प्रस्तुत काव्यांश में बच्चे द्वारा चाँद माँगने के लिए की जाने वाली सहज चेष्टा एवं बाल-सुलभ हठ का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। बच्चे को मनाने के क्रम में माँ द्वारा दर्पण में चाँद दिखलाना अत्यंत स्वाभाविक है, जिसका प्रयोग वर्षों से अनेक माताएँ अपने बच्चे को बहलाने के लिए करती आईं हैं। अक्सर माताएँ अपने अबोध शिशुओं के हठ को इसी प्रकार के उपायों से शांत करती हैं। काव्यांश में वात्स्लय रस है।
(ख) काव्यांश की भाषा सरल, सुबोध एवं आकर्षक है, जिसमें सजीवता का गुण भी मौजूद है। उर्दू-हिंदी मिश्रित लोकभाषा अर्थात् स्थानीय बोली के अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है; जैसे-ज़िदयाया, हई, देके, पै आदि। चित्रात्मक शैली एवं बिंब प्रधान भाषा अपनी स्वाभाविकता के कारण अत्यंत आकर्षक बन पड़ी है।
यह काव्यांश उर्दू एवं फ़ारसी के एक छंद ‘रुबाई’ में लिखा गया है। इस छंद में चार पंक्तियाँ होती हैं, जिसकी पहली, दूसरी एवं चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, जबकि तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है।
(ग) काव्यांश में प्रयुक्त काव्य-पंक्ति ‘देख आईने में चाँद उतर आया है’ में एक सरल एवं सहज माँ की स्वाभाविक सूझ-बूझ की प्रवृत्ति की झलक मिलती है। बालक द्वारा चाँद लेने की ज़िद करने पर माँ आईने में उसे चाँद की परछाईं दिखाती है। इस पूरे उपक्रम में ग्रामीण संस्कृति एवं ग्रामीण स्त्रियों की रचनात्मक काल्पनिकता मुखरित हो उठी है।
उत्तर 10.
(क) ‘आत्म परिचय’ कविता की प्रथम पंक्ति में कवि कहता है-”मैं जग-जीवन का भार लिए फिरता हूँ”, जबकि आगे की पंक्तियों में उसका कथन है-”मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ।” वस्तुतः ये दोनों पंक्तियाँ परस्पर विरोधाभासी लगती हैं, जो इस बात का परिचायक है कि संसार से हमारा रिश्ता दो विरोधी प्रवृत्तियों-प्रीति एवं कलह से एक समान है। संसार का भार हमारे मन-मस्तिष्क पर निश्चित रूप से पड़ता है। यह दुनिया अपने व्यंग्य-बाणों, तौर-तरीकों एवं शासन-प्रशासन से मनुष्य को चाहे जितना भी कष्ट दे, किंतु मनुष्य इससे पूरी तरह कटकर रह ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया से ही, इस समाज से ही मनुष्य का अस्तित्व है। यही हमारा उत्स एवं हमारी अस्मिता है। कवि सांसारिकता की प्रवृत्तियों से उभरे कष्ट के बाद मुक्ति की आकांक्षा पालता है। संसार के प्रति आसक्ति का अभाव और संसार के निवासियों के प्रति प्यार ही इन पंक्तियों का आशय है।
(ख) ‘कैमरे में बंद अपाहिज’ कविता संवेदनहीन सूचना प्रसारण तंत्र पर एक गहरा व्यंग्य है। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर किसी अपाहिज की पीड़ा को जनसंचार माध्यमों के द्वारा आमजनों तक पहुँचाने वाला व्यक्ति उसके दुःख-दर्द को बेचने का काम करता है। उसे न तो अपाहिजों के प्रति वास्तविक संवेदना है और न उनके मान-सम्मान के प्रति चिंता। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न बेहद अपमानजनक होते हैं। जो प्रसारण तंत्र की संवेदनहीनता को ही उजागर करते हैं। वास्तव में, मीडिया (दूरदर्शन) द्वारा एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने का उद्देश्य सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर व्यक्ति की दीनता एवं बेबसी को बेचकर अपने दर्शकों की संख्या में वृद्धि करके पैसा कमाना है।
(ग) प्रस्तुत काव्य पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने भक्ति की रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए राम की भक्ति के बल पर जाति-पाँति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस दिखाया है। रामभक्त तुलसी अपने युग की विषमताओं से डरते नहीं हैं, क्योंकि वे रामभक्ति में आकंठ डूबे हुए हैं। अतः वे स्वाभिमान एवं निडरता का परिचय देते हुए कहते हैं कि मुझे अपना संसार बिगड़ने का कोई भय नहीं है और न ही मुझे किसी से धन, संपत्ति या आश्रय पाने की चाह है। मैं तो लोगों से माँगकर खाने में ही संतुष्ट हूँ। मुझे मस्जिद में सोने से भी कोई परहेज़ नहीं है। मैं तो राम के भरोसे निश्चित हूँ। यहाँ तुलसीदास ने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं का ज़ोरदार खंडन तथा मस्जिद में सोने की बात कहकर धार्मिक संकीर्णताओं की धज्जियाँ उड़ा दी हैं।
उत्तर 11.
(क) भारतीय कला के बारे में लेखक का मानना है कि भारतीय कला को सौंदर्यशास्त्र एवं कई रसों की अच्छी समझ व उन पर अच्छी पकड़ है, जिसका प्रमाण अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। भारतीय कलाकृतियों का सौंदर्यशास्त्र के विभिन्न प्रतिमानों पर खरा उतरना तथा उनमें विभिन्न रसों का पाया जाना श्रेष्ठता का सूचक है, किंतु भारतीय कला में करुणा और हास्य की एक साथ प्रस्तुति नहीं मिलती अर्थात् करुणा और हास्य को एक-दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जाता।
(ख) भारतीय साहित्य के संस्कृत नाटकों में हास्य अभिनेता को ‘विदूषक’ कहा जाता है। यह राजा का अत्यंत विश्वस्त पात्र होता है, जो अपने वाक्चातुर्य से राजा एवं दरबारियों का मनोरंजन करता है। यह अपने पेटूपन या बेतुकी बातों के माध्यम से लोगों के दिलों में हास्य की भावना उत्पन्न करके उनका स्वस्थ मनोरंजन करता है।
(ग) भारतीय संस्कृति में करुणा का हास्य में बदले जाने एवं स्वयं पर हँसने वाली परंपरा सामान्यतः दिखाई नहीं देती। हमारे समाज में दूसरों पर तो हँसा जाता है, लेकिन स्वयं को हँसी का पात्र नहीं बनाया जाता। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय महाकाव्यों-रामायण एवं महाभारत में भी दूसरों पर हँसने की परंपरा है, स्वयं पर नहीं।
(घ) भारतीय साहित्य में करुणा व हास्य के सामंजस्य का अभाव दिखता है। इनकी रचना लोकमंगल हेतु की जाती है, जहाँ पाठक को आनंद प्रदान करना उद्देश्य तो है, लेकिन वह पारलौकिक या चित्त शांति का आनंद प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जहाँ थोड़ा-बहुत हास्य है भी, वह स्वयं से संबंधित न होकर दूसरों पर हँसने से संबंधित है। भारतीय साहित्य करुणा को हास्य में बदलने के आनंद से वंचित है।
उत्तर 12.
(क) ‘लक्ष्मी’ का जीवन दुःखों से भरा था। जब वह केवल 36 वर्ष की थी, तभी वह विधवा हो गई थी। पति की मृत्यु के उपरांत उसके ससुराल वाले उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे, इसलिए वे उसकी दूसरी शादी के लिए ज़ोर देने लगे, परंतु लक्ष्मी ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने अपने बड़े दामाद को घरजमाई बनाकर रखा, परंतु वह भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने घर में धन का अभाव रहने के कारण वह एक बार लगान भी समय पर न चुका पाई, जिसके कारण उसे धूप में खड़े रहने की सज़ा मिली। इस अपमान को सहन न कर सकने के कारण वह अपना गाँव छोड़कर शहर आ गई और लेखिका के यहाँ सेविका बन गई। उसकी वेशभूषा देखकर लेखिका ने उसका नाम ‘भक्तिन’ रख दिया। इस प्रकार, ‘लक्ष्मी’ के ‘भक्तिन’ बनने की प्रक्रिया यथार्थ में अत्यंत मर्मस्पर्शी है।
(ख) बाज़ार में सभी जाति, धर्म एवं लिंग के व्यक्ति आते हैं और वे अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार, वस्तुएँ खरीदते हैं। बाज़ार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है। बाज़ार में व्यक्ति की महत्ता उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। विक्रेता उसी ग्राहक को महत्त्व देता है, जो अधिक खरीदारी करता है। इस दृष्टि से जाति-धर्म का भेद मिटाकर बाज़ार सामाजिक समरसता की रचना करता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि बाज़ार सभी प्रकार की असमानताओं को भूलकर सामाजिक समरसता को स्थापित करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
(ग) ‘काले मेघा पानी दे’ पाठ में लेखक की जीजी इंदर सेना पर पानी फेंका जाना सही ठहराती है, जबकि लेखक अपनी जीजी की बात से बिलकुल भी सहमत नहीं दिखता।
लेखक की जीजी अपनी बात या विचार के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देती हैं।
जब हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए पहले चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। इसी उद्देश्य से हम पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं, क्योंकि जीवन में हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए पहले अर्घ्य नहीं चढ़ाएँगे अर्थात् देंगे नहीं तो उसे पाएँगे कैसे?
- मनुष्य को पहले त्याग करना चाहिए और फिर फल की आशा रखनी चाहिए। त्याग उसी वस्तु का मान्य होता है, जिसकी त्याग करने वाले को भी बहुत आवश्यकता होती है। पानी के संदर्भ में भी यही स्थिति है।
- जीजी ने खेत में गेहूं की अच्छी फ़सल पाने के लिए अच्छे बीजों को डालने का तर्क देकर भी अपनी बात को सही ठहराया अर्थात् इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को सही बताया।
(घ) फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ की ‘पहलवान की ढोलक’ कहानी में लेखक ने गाँव की उस चिरपरिचित अवस्था का भावपूर्ण चित्रण किया है, जिसमें गाँववासी अपनी भावनाओं से ही एक-दूसरे की सहायता कर पाते हैं, क्योंकि वे आर्थिक रूप से इतने समर्थ नहीं होते कि किसी की आर्थिक सहायता कर सकें। जब महामारी से विभिन्न घरों में एक-दो लाशें लगातार निकलनी शुरू हो गईं, तो वे मानसिक एवं आर्थिक रूप से इतने टूट गए कि कफ़न तक के लिए प्रबंध करना भी उनके लिए मुश्किल होने लगा। उन्हें कफ़न का इंतज़ाम करने के लिए सोचना पड़ रहा था।
यही कारण है कि गाँव वाले अपने पड़ोसियों को बिना कफ़न के ही लाशों को पानी में बहा देने की सलाह देने लगे, क्योंकि सभी की आर्थिक स्थिति अत्यधिक बदतर हो गई थी।
(ङ) ‘नमक’ कहानी स्पष्ट करती है कि राजनैतिक सीमा तथा सत्ता लोलुपता व मज़हबी दुराग्रहों में बँटे होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के दिलों में विभाजन की भावना या किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। यह एक सच्चाई है कि सामान्य जनता धर्म या क्षेत्र के आधार पर विभाजन पसंद नहीं करती है। भारतीय सिख बीबी लाहौर का नमक, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली की जामा मस्जिद तथा भारत के कस्टम अधिकारी ढाका के नारियल को अभी तक नहीं भूले हैं। वस्तुतः वे सब मिल-जुलकर रहना चाहते हैं, उनके दिलों में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक चालों ने उनकी इच्छाओं का दमन कर दिया और वे उस राजनीतिक परिस्थिति के शिकार बन गए, जिसने गंगा-जमुनी संस्कृति को विभाजित कर दिया। यह विभाजन अभी तक दिलों पर हावी नहीं हो पाया है।
उत्तर 13.
‘सिल्वर वैडिंग’ कहानी में स्थिति को ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लेना व अनिर्णय की स्थिति का द्वंद्व प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू एक साधारण व्यक्ति हैं, जिनके व्यक्तित्व पर किशन दा का अत्यधिक प्रभाव है। किशन दा ने ही यशोधर बाबू को जीवन के कठिन समय में सभी प्रकार से सहारा दिया था। यशोधर बाबू के मन एवं मस्तिष्क पर उनका इतना अधिक प्रभाव था कि वे किशन दा की तरह ही सोचते थे। वे भी संयुक्त परिवार को ही अच्छा मानते थे तथा अपने संबंधियों की सहायता करना अपना फ़र्ज समझते थे। उनके बच्चे पढ़-लिखकर अच्छा वेतन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन यशोधर बाबू उनके कहने पर भी अपनी सादगी को नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी पत्नी चाहती थी कि वे भी समय के साथ ढल जाएँ, परंतु यशोधर बाबू स्वयं को बदलना नहीं चाहते थे। बच्चों के कहने पर यशोधर बाबू की पत्नी ने शादी की 25वीं वर्षगाँठ पर पार्टी करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन ऑफिस में यशोधर बाबू से सहकर्मियों द्वारा दावत माँगे जाने पर वे केवल मिठाई खाने के लिए कुछ रुपये ही देते हैं।
घर पर आयोजित अपनी ही पार्टी में वे अनमने ढंग से शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते। इस प्रकार अनेक स्थितियाँ ऐसी आती हैं, जब यशोधर बाबू को न चाहते हुए भी ढलना पड़ता है। वस्तुतः वे अनिर्णय की स्थिति से बाहर नहीं आ पाते। इस प्रकार संपूर्ण कहानी परंपरागत जीवन शैली और आधुनिक विचारधाराओं से प्रेरित जीवन शैली से उत्पन्न द्वंद्व के बीच रची-बसी है।
उत्तर 14.
(क) नदी, कुएँ, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी व्यवस्था को देखते हुए सिंधु घाटी सभ्यता को ‘जल संस्कृति’ कहा जा सकता है। आज के ग्रामीण एवं शहरी समाज के सामने एक बड़ी समस्या जल की उपलब्धता एवं उसकी निकासी से जुड़ी हुई है, लेकिन हज़ारों वर्ष पूर्व की सिंधु सभ्यता में जल का प्रबंधन अत्यंत उच्च स्तरीय था।
सिंधु घाटी सभ्यता में सामूहिक स्नान के लिए बने स्नानागार उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण होने के साथ-साथ तत्कालीन जल प्रबंधन की उत्कृष्टता को भी दर्शाते हैं। एक पंक्ति में आठ स्नानघर हैं, जिनमें किसी का भी द्वार एक-दूसरे के सामने नहीं खुलता है। पानी के जमाव वाले कुंड के तल में तथा दीवारों पर ईंटों के बीच चूने एवं चिराड़ी के गारे का प्रयोग हुआ है, जिससे कुंड का पानी रिसकर बाहर न आ सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न जा सके।
सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों के साथ बनी हुई नालियाँ पक्की ईंटों से ढकी हैं। यह जल निकासी का सुव्यवस्थित बंदोबस्त है। आधुनिक वास्तुकार भी सिंधु सभ्यता की इस व्यवस्था की उत्कृष्टता एवं महत्त्व को स्वीकार करते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता को उच्च स्तरीय सभ्यता के रूप में पहचान बनाने में वहाँ के ‘जल प्रबंधन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। अतः सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति’ के रूप में भी देखा जा सकता है।
(ख) जूझ’ कहानी में कथा नायक ने मुख्यतः अपनी पढ़ाई के प्रति जूझने की भावना को उजागर किया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि लेखक को पढ़ाई जारी रखने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ा। लेखक के पिता बहुत आलसी और गैर-ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं। वह लेखक को पाठशाला नहीं भेजते थे, क्योंकि यदि लेखक पाठशाला चला जाएगा, तो खेत का काम कौन करेगा? वे स्वयं दिनभर गाँव में घूमते रहते और रखमाबाई के कोठे पर भी जाते, जबकि लेखक को खेत के काम में लगाए रखना चाहते थे।
गाँव के एक प्रभावशाली व्यक्ति दत्ता जी राव के कहने पर उन्होंने लेखक को पाठशाला तो भेजा, लेकिन अपनी कुछ शर्तों के साथ। उनकी शर्ते थीं कि लेखक सुबह के ग्यारह बजे तक खेतों में पानी देकर फिर पाठशाला जाएगा और पाठशाला से आकर फिर एक घंटा पशुओं को चराएगा। यदि किसी दिन खेत में अधिक काम होगा, तो उस दिन वह पाठशाला से छुट्टी ले लेगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी लेखक ने अपने पढ़ने का जुनून नहीं छोड़ा। पाठशाला में भी लड़कों ने उसकी खिल्ली उड़ाई, क्योंकि वह मटमैली धोती एवं गमछा पहनकर गया था। धीरे-धीरे लेखक ने अपने परिश्रम एवं लगन के बल पर अपने अध्यापकों एवं सहपाठियों का दिल जीत लिया। लेखक प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ पढ़ाई भी करता है और खेत का काम भी सँभालता है।
इस प्रकार यह कहानी हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की प्रेरणा देती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं से जूझना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।
We hope the CBSE Sample Papers for Class 12 Hindi Paper 3 help you. If you have any query regarding CBSE Sample Papers for Class 12 Hindi Paper 3, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.