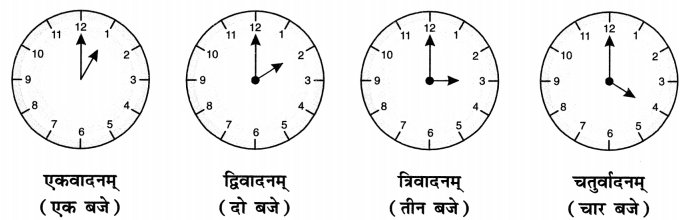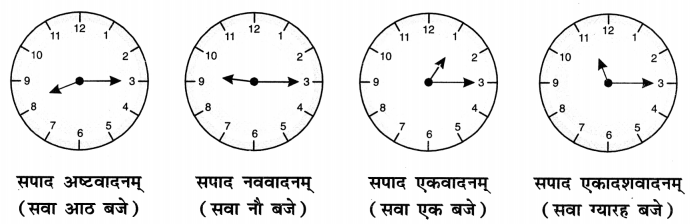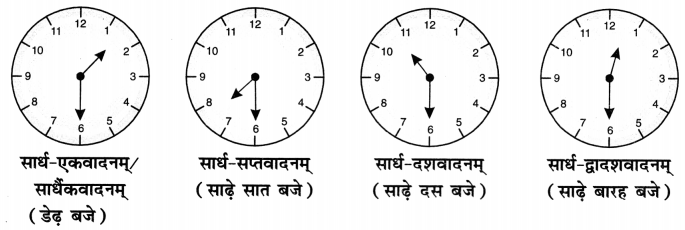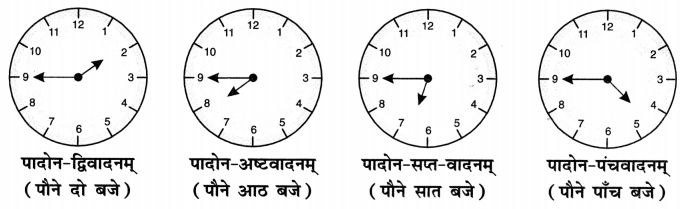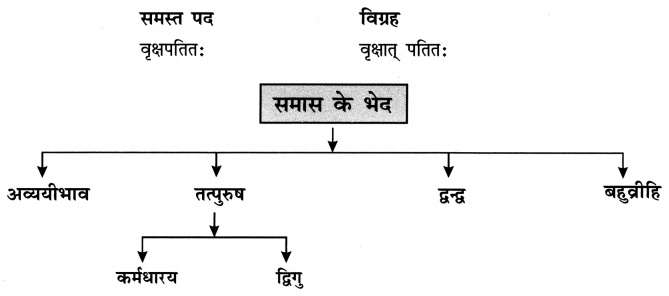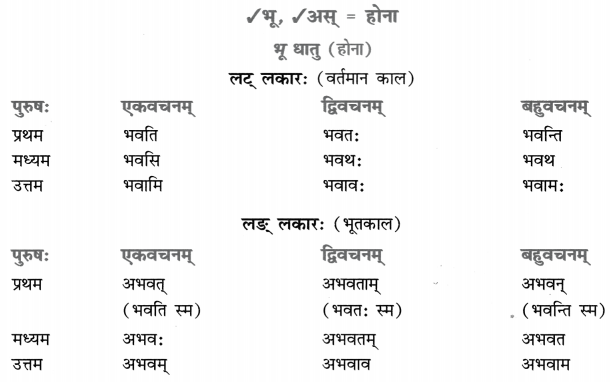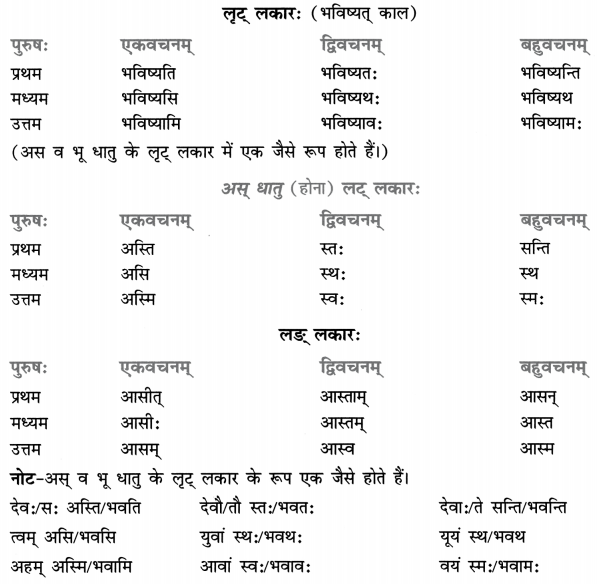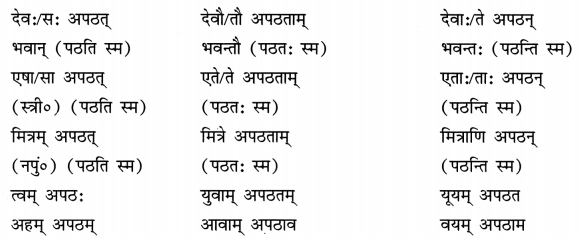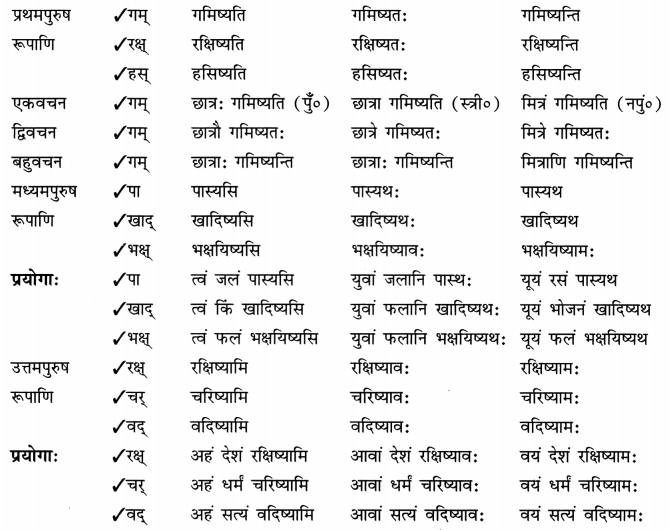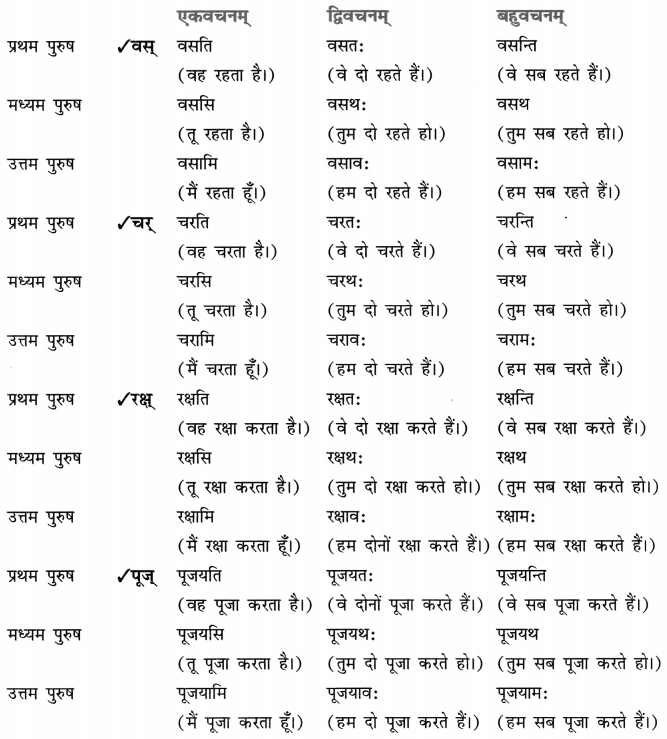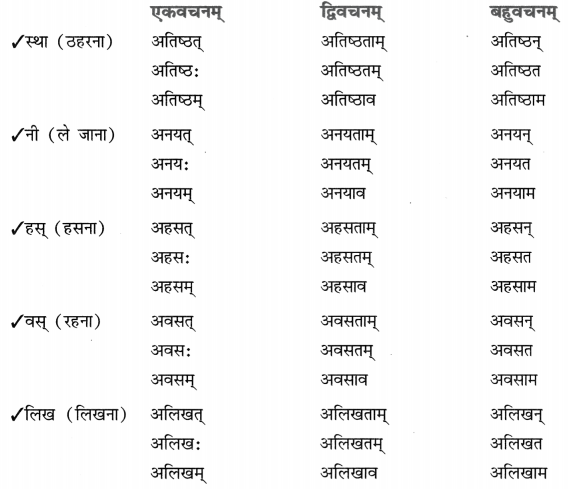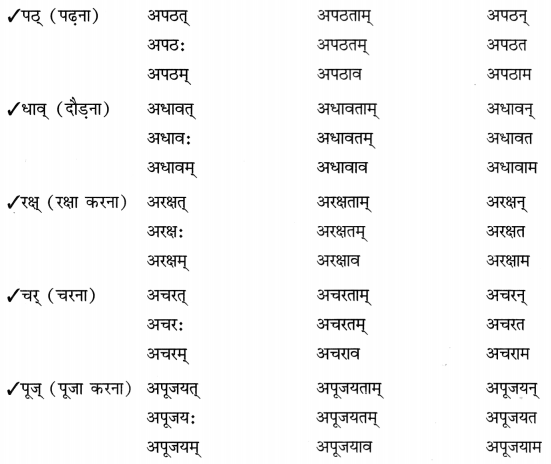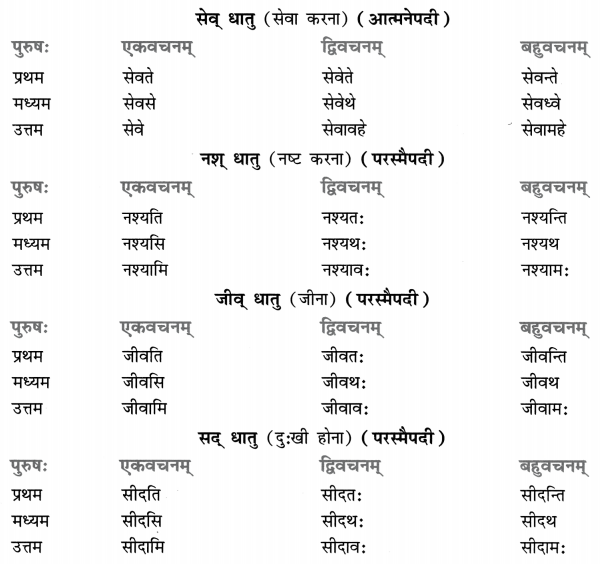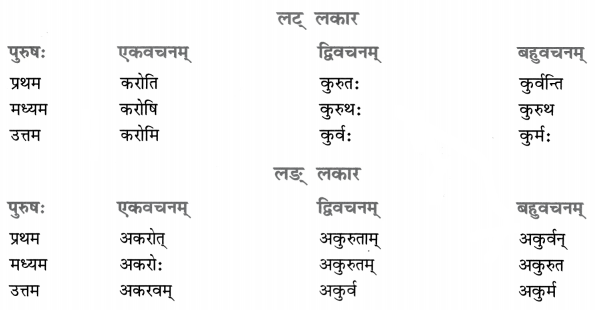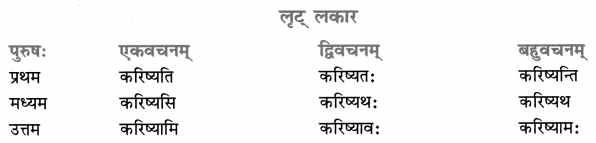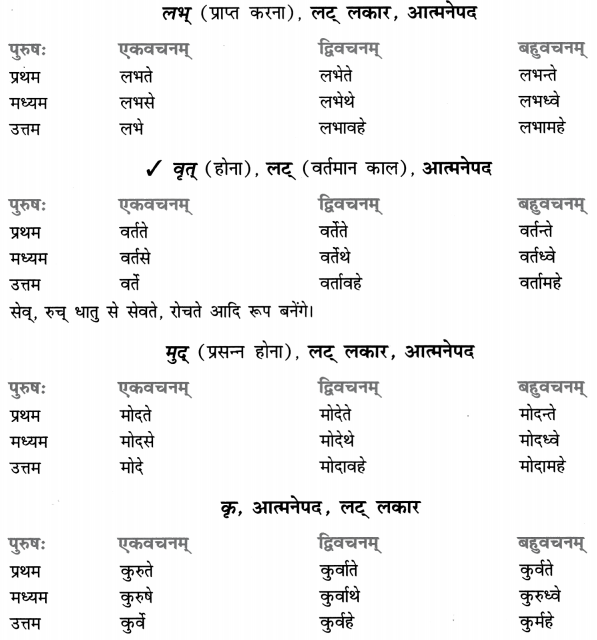We have given detailed NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit Grammar Book कारक व उपपद विभक्तियाँ Questions and Answers come in handy for quickly completing your homework.
Sanskrit Vyakaran Class 8 Solutions कारक व उपपद विभक्तियाँ
वाक्य में क्रिया के साथ जिस शब्द का साक्षात् सम्बन्ध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे- रमा चलति, देवः पठति। संस्कृत में छ: कारक होते हैं-
- कर्ता
- कर्म
- करण
- सम्प्रदान
- अपादान
- अधिकरण
संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना गया है क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। सम्बोधन के शब्द कर्ता कारक के समान ही होते हैं इसलिए, इन्हें अलग से कारकों में नहीं गिना जाता। संस्कृत में दो प्रकार की विभक्तियाँ हैं-
- कारकविभक्तिः
- उपपदविभक्तिः
जब क्रिया के विचार से विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे ‘कारक विभक्ति’ कहते हैं। जैसेरविः कलमेन लिखति। यहाँ ‘कलमेन’ में ‘करण’ के कारण तृतीया विभक्ति है, किन्तु ‘बालकाः मोहनेन सह पठन्ति’, यहाँ मोहनेन में तृतीया ‘सह’ अव्यय के कारण है। अतः जब अव्यय या किसी विशेष कारण से किसी विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे ‘उपपद विभक्ति’ कहते हैं। जैसे–’सह’ के योग से तृतीया-विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है।
कारक-विभक्तिः
- कर्ता कारक – कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे- अहम् पुस्तकं पठामि। सीता पठति।
- कर्म कारक – कर्ता को जो करना अभीष्ट होता है, या जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं। जैसे- रामः पत्रं लिखति।
- करण कारक – जिस साधन से कार्य सम्पन्न होता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे- बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति।
- सम्प्रदान कारक – कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है उसे सम्प्रदान कहते हैं। जैसे- माता पुत्राय वस्त्राणि आनयति।
- अपादान कारक – जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु या स्थान से जुदाई पाई जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे- वृक्षात् पत्राणि पतन्ति।
- सम्बन्ध – संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कहलाते हैं। जैसे- इदम् मम पुस्तकम् अस्ति।
- अधिकरण कारक – क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे- छात्राः विद्यालये पठन्ति।
उपपद-विभक्तिः
संस्कृत में कुछ ‘विना’, ‘सह’ आदि अव्यय शब्द हैं। उनके साथ निश्चित विभक्ति का प्रयोग होता है। जब इस प्रकार के शब्दों के आधार पर विभक्ति लगाई जाती है तो उसे उपपद-विभक्ति कहते हैं।
द्वितीया – प्रति, परितः, उभयतः, विना, अभितः के योग में-
- प्रति – (की ओर) – वृद्धः उद्यानं प्रति गच्छति।
- उभयतः, अभितः – (दोनों ओर) – नगरम् उभयतः वृक्षाः सन्ति।
- परितः – (चारों ओर) – कृष्णम् परितः (अभितः) गोपाः सन्ति।
- विना – (बगैर) – सीता राम विना वनं न गच्छति।
(प्रच्छ्, याच्, कथ्, नी, गम्, रक्ष, धिक् तथा नम् आदि धातुओं के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है।)
तृतीया – सह, साकं, सार्धम्, विना, हीन तथा अलम् आदि के योग में-
- सह, साकं, सार्धम् – (साथ-साथ) – पुत्रः जनकेन सह (साकं, साधम्) भ्रमति।
- विना – (बगैर) – सीता रामेण विना वनं न गच्छति।
- हीन – (रहित) – सः धनेन हीनः अस्ति।
- अलम् – (मत / बस) – अलम् कोलाहलेन।
(इसके अतिरिक्त सदृशं, समम्, तुल्य तथा अंग विकार बताने वाले शब्दों के योग में भी तृतीया होती है।)
चतुर्थी – नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम्, रुच् तथा क्रुध् के योग में-
- नमः – (नमस्कार) – नमः शिवाय।
- स्वस्ति – (कल्याण हो) – प्रजाभ्यः स्वस्ति।
- स्वाहा – (देवताओं की आहुति) – अग्नये स्वाहा।
- अलम् – (काफी, पर्याप्त) – एतद् दुग्धं बालकाय अलम्।
- रुच् – (अच्छा लगना) – मह्यम् मोदकं रोचते।
- क्रुध् – (क्रोध करना) – पिता पुत्राय क्रुध्यति।
(इसके अतिरिक्त स्पृह तथा स्वधा के योग में भी चतुर्थी होती है।)
पंचमी – ऋते, बहिः, अनन्तरम्, पूर्वम्, प्रभृति, प्र + भू और भी के योग में-
- ऋते – (बिना) – विद्यायाः ऋते न ज्ञानम्।
- बहिः – (बाहर) – छात्रः कक्षायाः बहिः तिष्ठति।
- अनन्तरम् – (के बाद) – सायंकालात् अनन्तरम् अन्धकारः भवति।
- पूर्वम् – (पूर्व दिशा) – नगरात् पूर्वम् नदी वहति।
- प्रभृति – (से लेकर) – सः शैशवात् प्रभृति चतुरः।
- प्र + भू – (पैदा होना) – गंगा हिमालयात् प्रभवति।
- भी – (डरना) – बालः सिंहात् बिभेति।
षष्ठी – निर्धारण में, उपरि, अधः, पृष्ठतः, पुरतः, पश्चात् के योग में-
- निर्धारण में – (बहुतों में से एक को कम या अधिक बताना) – रामः बालकेषु/बालकानाम् श्रेष्ठः।
तुलनात्मक- वर्णन के कारण षष्ठी या सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। - उपरि – (ऊपर) – पुस्तकं पटलस्य उपरि अस्ति।
- अधः – (नीचे) – भूमेः अधः जलम् अस्ति।
- पृष्ठतः – (पीछे से) – तस्य पुत्रः गृहस्य पृष्ठतः अधावत्।
- पुरतः – (सामने से) – मम पुरतः मा तिष्ठ।
- पश्चात् – (बाद में) – भोजनस्य पश्चात् सः विश्रामं करोति।
सप्तमी – निपुण, कुशल, प्रवीण, विश्वास और स्नेह के योग में-
- निपुण – (चतुर) – सः अध्ययने निपुणः अस्ति।
- कुशल – (चतुर, प्रवीण) – अर्जुनः युद्धे कुशलः आसीत्।
- प्रवीण: – (होशियार) – रमेशः वीणावादने प्रवीणः।
- वि + श्वस् – (विश्वास करना) – गुरुः शिष्ये विश्वसिति।
- स्निह् – (स्नेह करना) – पुत्रे स्निह्यति माता। पिता पुत्रे स्निह्यति।
बहुविकल्पीय प्रश्नाः
1. ‘प्रति’ शब्दस्य योगे का विभक्तिः प्रयुक्ता भवति?
(क) द्वितीया
(ख) चतुर्थी
(ग) सप्तमी
(घ) प्रथमा
उत्तराणि:
(क) द्वितीया
2. रेखांकित पदे का विभक्तिः किं च वचनम्?
मह्यम् भ्रमणं रोचते।
(क) द्वितीया, एकवचन
(ख) सप्तमी, बहुवचन
(ग) चतुर्थी, एकवचन
(घ) षष्ठी, बहुवचन
उत्तराणि:
(ग) चतुर्थी, एकवचन
3. प्रकोष्ठे प्रदत्तशब्दस्य समुचितरूपेण रिक्तस्थानं पूरयत-
पुत्रः ___________ सह गच्छति।
(क) जनकः
(ख) जनकस्य
(ग) जनकेन
(घ) जनकम्
उत्तराणि:
(ग) जनकेन
4. रेखांकितपदे का विभक्तिः कि च वचनं?
धनात् ऋते न सुखम्
(क) तृतीया एकवचन
(ख) पंचमी, एकवचन
(ग) सप्तमी, बहुवचन
(घ) द्वितीया, एकवचन
उत्तराणि:
(ख) पंचमी, एकवचन
5. ‘विना’ शब्दस्य योगे का विभक्तिः प्रयुक्ता भवति?
(क) तृतीया
(ख) षष्ठी
(ग) चतुर्थी
(घ) सप्तमी
उत्तराणि:
(क) तृतीया
6. उचितपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-
(i) सैनिकाः ___________ रक्षन्ति।
(क) देशः
(ख) देशम्
(ग) देशस्य
(घ) देशे
उत्तराणि:
(ख) देशम्
(ii) सः ___________ काणः।
(क) नेत्राः
(ख) नेत्राभ्याम्
(ग) नेत्रेण
(घ) नेत्रः
उत्तराणि:
(ग) नेत्रेण
(iii) बालकः ___________ बिभेति।
(क) सिंहस्य
(ख) सिंहम्
(ग) सिंहः
(घ) सिंहात्
उत्तराणि:
(घ) सिंहात्
(iv) पिता ___________ क्रुध्यति।
(क) पुत्राय
(ख) पुत्रम्
(ग) पुत्रेभ्यः
(घ) पुत्रस्य
उत्तराणि:
(क) पुत्राय
(v) माता-पिता ___________ विश्वसतः।
(क) बालकाः
(ख) बालकेषु
(ग) बालको
(घ) बालकाभ्याम्
उत्तराणि:
(ख) बालकेषु
7. निम्नलिखित वाक्येषु रेखांकितपदे का विभक्तिः प्रयुक्ता-
(i) अध्यापकः छात्रे स्निह्यति।
(क) सप्तमी
(ख) षष्ठी
(ग) तृतीया
(घ) पंचमी
उत्तराणि:
(क) सप्तमी
(ii) गुरुः शिष्यम् प्रश्नम् पृच्छति।
(क) प्रथमा
(ख) तृतीया
(ग) षष्ठी
(घ) द्वितीया
उत्तराणि:
(घ) द्वितीया
8. शुद्धं पदं कोष्ठकात् चित्वा समक्षं प्रदत्तस्थाने लिखत-
- ___________ पत्राणि पतन्ति। (वृक्षात्, वृक्षस्य)
- गंगा ___________ प्रभवति। (हिमालयात्, हिमालयः)
- अलम् ___________। (रोदनात्, रोदनेन)
- छात्रः ___________ प्रति गच्छति। (नगरं, नगरस्य)
- ___________ स्वाहा। (इन्द्रं, इन्द्राय)
- ___________ विना जीवनम् वृथा। (जलस्य, जलम्)
- सः ___________ निपुणः। (कार्ये, कार्यस्य)
- ___________ उभयतः जलम् वहति। (देशम्, देशस्य)
- ___________ मिष्टान्नं रोचते। (बालकस्य, बालकाय)
- रामः अद्य ___________ बहिः अगच्छत्। (ग्रामात्, ग्रामस्य)
उत्तराणि:
- वृक्षात्
- हिमालयात्
- रोदनेन
- नगरम्
- इन्द्राय
- जलम्
- कार्ये
- देशम्
- बालकाय
- ग्रामात्